भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय “ज्ञान कर्म संन्यास योग” कहलाता है।यह अध्याय हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संतुलन हो।
- परिचय:
- प्रमुख विषय-वस्तु:
- अध्याय का सारांश:
- अंतिम श्लोक:
- निष्कर्ष:
- भगवद गीता – चतुर्थ अध्याय (ज्ञान कर्म संन्यास योग) से हमें क्या सीख मिलती है?
- निष्कर्ष:
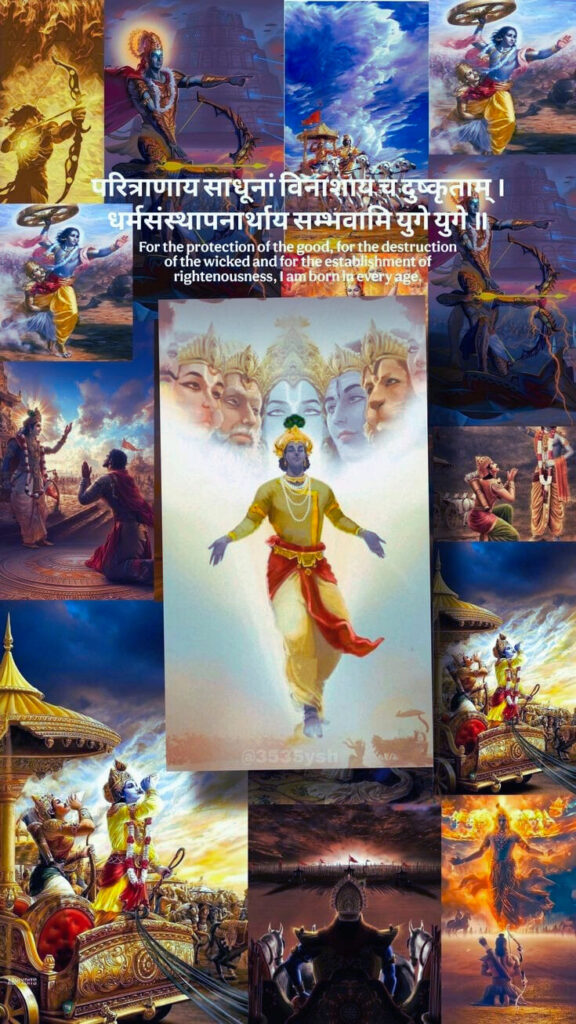
परिचय:
भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय “ज्ञान कर्म संन्यास योग” कहलाता है। यह अध्याय अर्जुन और श्रीकृष्ण के संवाद की उस कड़ी का विस्तार है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान, और भक्ति का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान यह बताते हैं कि किस प्रकार से कर्म करते हुए भी मनुष्य ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर सकता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
प्रमुख विषय-वस्तु:
इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं और इसकी विषयवस्तु निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं में विभाजित की जा सकती है:
- भगवान का दिव्य आविर्भाव (अवतार)
- ज्ञान का उत्तराधिकार और उसका ह्रास
- कर्म और ज्ञान का समन्वय
- कर्म का त्याग और निष्काम भाव
- ज्ञान की महत्ता और गुरु की आवश्यकता
- ज्ञान यज्ञ और विभिन्न प्रकार के यज्ञ
- अज्ञान का नाश और आत्मबोध
- कर्मबन्धन से मुक्ति और ब्रह्म में स्थित अवस्था
1. दिव्य आविर्भाव और श्रीकृष्ण का अवतार सिद्धांत:
भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान पहले सूर्यदेव (विवस्वान) को दिया था, विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। यह परंपरा से ऋषियों और राजाओं तक पहुँचा, परंतु समय के साथ यह लुप्त हो गया।
श्रीकृष्ण कहते हैं:
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽअत्मानं सृजाम्यहम्॥”
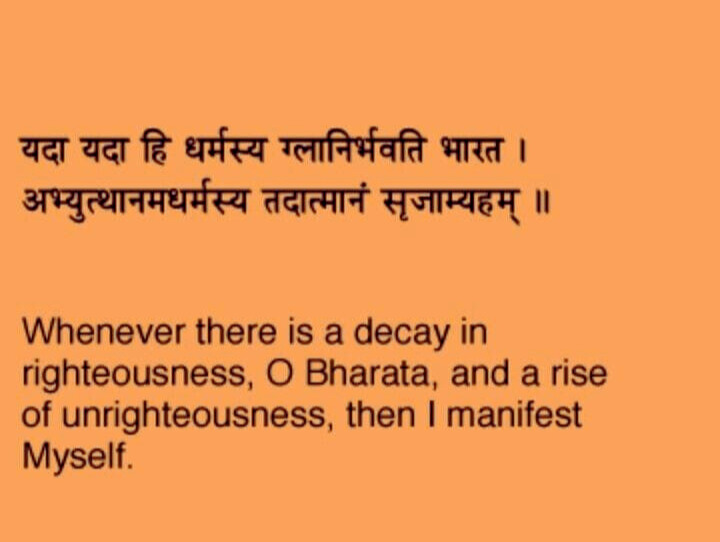
जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने आप को (अवतार रूप में) प्रकट करता हूँ।
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥”
सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश, और धर्म की स्थापना हेतु मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ।
यहाँ श्रीकृष्ण अपने दिव्य जन्म को ‘अविनाशी और अजन्मा’ होते हुए भी ‘माया’ द्वारा जन्म लेने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य (अलौकिक) है और जो मनुष्य इसे तत्व से जान लेता है, वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है।
2. कर्म, ज्ञान और उनका समन्वय:
श्रीकृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वे कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं हैं, फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि संसार का संतुलन बना रहे और लोग उनके आचरण का अनुकरण करें। यही कर्मयोग का सिद्धांत है – बिना फल की इच्छा किए कार्य करना।
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।”
इस अध्याय में यह भाव गहराई से व्याप्त है – कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, और ज्ञान के साथ अपने कर्म को संयमित करो।
3. निष्काम कर्म और कर्म का परित्याग:
यहाँ पर श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का परित्याग करने से नहीं बल्कि कर्म करते हुए ज्ञान के माध्यम से उसमें आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। वे कहते हैं कि:
“कर्मज्ञं तम् आहुः पण्डिता यं कर्मणः फलं त्यक्त्वा।”
जो व्यक्ति कर्मों में निहित अकर्ता को पहचानता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। अर्थात वह कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता।
4. ज्ञान की महिमा:
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वह अग्नि है, जो समस्त कर्मों को भस्म कर देती है।
“यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥”
यहाँ ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि यह ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता और सेवा-भाव के साथ गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करता है।
5. गुरु की महत्ता:
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥”
ज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछो, सेवा करो। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानीजन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे।
यह श्लोक भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा का स्तंभ माना जाता है।

6. विभिन्न प्रकार के यज्ञ:
श्रीकृष्ण बताते हैं कि यज्ञ के अनेक प्रकार हैं – द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। लेकिन उन सभी में ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है।
“श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥” द्रव्य से किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ से कमतर है, क्योंकि सभी कर्मों का समापन ज्ञान में ही होता है
7. अज्ञान का नाश और आत्मबोध:
अंतिम भाग में श्रीकृष्ण यह बताते हैं कि जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है।
“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।”
इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। यह ज्ञान धीरे-धीरे साधना और अनुभव से प्राप्त होता है।
8. कर्मबंधन से मुक्ति और ब्रह्म स्थिति:
श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और आत्मसंयम से ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करता है, वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म में स्थित हो जाता है।
“योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय॥”
जिसका संशय ज्ञान से नष्ट हो चुका है, जो आत्मस्वरूप में स्थित है, उसे कर्म कभी नहीं बाँधते।
अध्याय का सारांश:
- ज्ञान और कर्म दोनों को एक साथ अपनाने की प्रेरणा दी गई है।
- कर्म करते हुए, फल की इच्छा त्याग देना ही सच्चा योग है।
- भगवान के दिव्य रूप और अवतार का रहस्य बताया गया है।
- गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा, और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट किया गया है।
- ज्ञान को सर्वोच्च पवित्रता का स्रोत बताया गया है।
अंतिम श्लोक:
“तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽत्मनः।
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥”
अर्जुन! इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञानजन्य संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काट डालो और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए उठ खड़े हो।
निष्कर्ष:
चतुर्थ अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण केवल कर्म, ज्ञान और संन्यास की व्याख्या नहीं करते, बल्कि आत्मा की शुद्धि, गुरुतत्त्व की आवश्यकता, और भक्ति से युक्त ज्ञान के मार्ग को विस्तार से समझाते हैं। यह अध्याय व्यक्ति को कर्म में लिप्त रहते हुए भी त्याग और वैराग्य के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है।
यह अध्याय उन साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है जो संसार में रहते हुए मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं और ईश्वर को कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से पाना चाहते हैं।

भगवद गीता – चतुर्थ अध्याय (ज्ञान कर्म संन्यास योग) से हमें क्या सीख मिलती है?
भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय “ज्ञान कर्म संन्यास योग” कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करते हुए भी आत्मज्ञान और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कई गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांत छिपे हैं, जो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।
1. ईश्वर का अवतार और उसका उद्देश्य:
इस अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे जब-जब धरती पर अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि देखते हैं, तब-तब वे अवतार लेते हैं।
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽअत्मानं सृजाम्यहम्॥”
इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म को समाप्त करने के लिए समय-समय पर स्वयं अवतरित होते हैं।
2. कर्म और फल की अपेक्षा का त्याग:
श्रीकृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करें और उसके फल से आसक्त न हों, तो वह कर्म बंधन नहीं बनता।
इससे हमें यह सिखने को मिलता है कि निष्काम कर्म (बिना किसी स्वार्थ के किया गया कार्य) सबसे श्रेष्ठ है और यही जीवन की सच्ची साधना है।
3. ज्ञान की महत्ता:
भगवान बताते हैं कि जैसे अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान सभी पापों और अज्ञान को नष्ट कर देता है।
“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।”
ज्ञान ही सबसे पवित्र साधन है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा, जीवन, ईश्वर और कर्म का सही ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। केवल कर्म या पूजा पर्याप्त नहीं है, जब तक उसमें सच्चा ज्ञान नहीं जुड़ा हो।
4. गुरु की आवश्यकता और विनम्रता:
श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है, उसे किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे विनम्रता, सेवा और श्रद्धा से प्रश्न पूछना चाहिए।
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।”
यह हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभवशील गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। सच्चे शिष्य का लक्षण है – विनम्रता, सेवा-भाव और सीखने की ललक।
5. संन्यास का सही अर्थ:
इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कर्म का त्याग करना ही संन्यास नहीं है, बल्कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा संन्यास है।
इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन से भागने का नाम संन्यास नहीं है, बल्कि जीवन के हर कर्म को भक्ति और ज्ञान के साथ करना ही सच्चा योग है।
6. संशय का नाश और आत्मविश्वास:
भगवान अंत में अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय में बसे अज्ञान और संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काटो और फिर निडर होकर अपने कर्मक्षेत्र में उतर जाओ।
“छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।”
यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, ज्ञान और ईश्वर पर विश्वास के साथ हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।
निष्कर्ष:
भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि:
- ईश्वर सदा हमारे साथ हैं और धर्म की रक्षा करते हैं।
- निष्काम कर्म ही जीवन का धर्म है।
- ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन ही मुक्ति का मार्ग है।
- गुरु की शरण में जाकर श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
- संशय और अज्ञान को त्यागकर हमें अपने जीवन-मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।
यह अध्याय हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संतुलन हो।

Pingback: Bhagavad Gita Chapter 5 - Good Health And Positive Thoughts